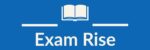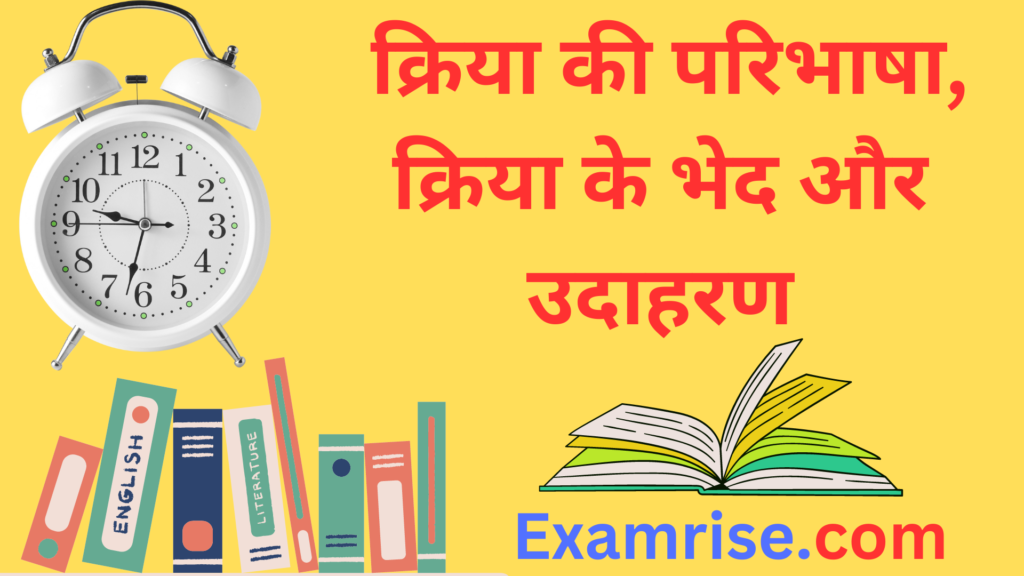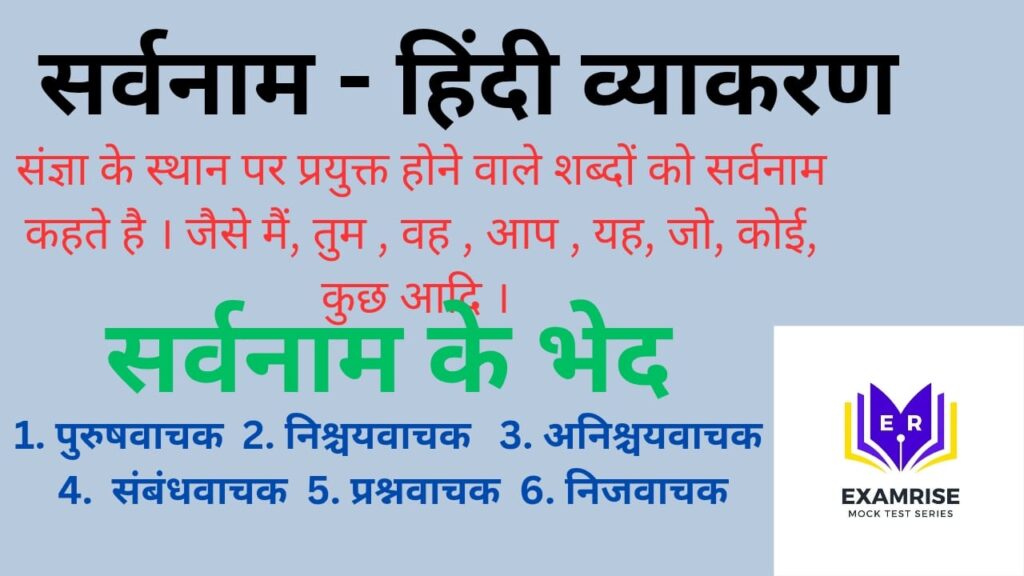वाक्य अशुद्धि शोधन की परिभाषा, वाक्य अशुद्धि शोधन के प्रकार और उदाहरण
Vaakya Ashudhhi Shodhan Definition, Examples, Types. वाक्य अशुद्धि शोधन की परिभाषा, वाक्य अशुद्धि शोधन के प्रकार और उदाहरण
Vaakya Ashudhhi Shodhan (वाक्य अशुद्धि शोधन) – इस लेख में हम वाक्य अशुद्धि शोधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। वाक्य अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? वाक्यों में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? और उन अशुद्धियों का शुद्ध रूप किस तरह होगा ये सब हम उदाहरणों की सहायता से जानेंगे –

वाक्य अशुद्धि शोधन
‘वाक्य’ भाषा की महत्त्वपूर्ण इकाई है, अत: वाक्य को बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य अर्थ भी बदल सकता है। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से और सही-सही समझ आ सके उसके लिए आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से ‘वाक्य’ को शुद्ध हो। अत: वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही ‘वाक्य अशुद्धि शोधन’ कहलाता है।
वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –
1. वर्तनी संबंधी अशुद्धि
वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द से सम्बंधित अशुद्धियाँ होती हैं। जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तो वहाँ उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है और आपका पूरा वाक्य अशुद्ध कहलाया जाता है।
उदाहरण –
इतिहासिक / एतिहासिक – अशुद्ध = ऐतिहासिक – शुद्ध
आशिर्वाद / आशिरवाद – अशुद्ध = आशीर्वाद – शुद्ध
उज्वल / उज्जवल – अशुद्ध = उज्ज्वल – शुद्ध
कवित्री / कवियत्री – अशुद्ध = कवयित्री – शुद्ध
2. शब्द-अर्थ प्रयोग की अशुद्धि
कभी-कभी वाक्यों में सही शब्दों की जगह उनके ही सादृश लगने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है, जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ ही बदल जाता है और यह वाक्य में शब्द-अर्थ प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है।
उदाहरण –
अशुद्ध रूप – मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे।
शुद्ध रूप – मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे।
अशुद्ध रूप – मैंने अपना ग्रहकार्य कर लिया है।
शुद्ध रूप – मैंने अपना गृहकार्य कर लिया है।
अशुद्ध रूप – तुम हमेशा बेफ़िजूल की बातें करते हो।
शुद्ध रूप – तुम हमेशा फ़िजूल की बातें करते हो।
3. लिंग संबंधी अशुद्धि –
कभी-कभी वाक्यों में लिंग संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं। ये वाक्य की लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाती हैं।
उदाहरण –
अशुद्ध रूप – बेटी पराए घर का धन होता है।
शुद्ध रूप – बेटी पराए घर का धन होती है।
अशुद्ध रूप – आज तुमने नया पोशाक पहना है।
शुद्ध रूप – आज तुमने नई पोशाक पहनी है।
अशुद्ध रूप – मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा।
शुद्ध रूप – मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी।
अशुद्ध रूप – कल मैंने नया पुस्तक ख़रीदा।
शुद्ध रूप – कल मैंने नई पुस्तक खरीदी।
4. वचन संबंधी अशुद्धि
कभी-कभी देखा गया है कि वाक्यों में वचन संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं। इन्हें वाक्य की वचन संबंधी अशुद्धि कहा जाता है।
उदाहरण –
अशुद्ध रूप – भारत में अनेकों राज्य हैं।
शुद्ध रूप – भारत में अनेक राज्य हैं।
अशुद्ध रूप – प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं।
शुद्ध रूप – प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है।
अशुद्ध रूप – इस समय चार बजा है।
शुद्ध रूप – इस समय चार बजे हैं।
अशुद्ध रूप – मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ।
शुद्ध रूप – मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ।
5. पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ
वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उसके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं रहती और इसे वाक्य की पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ कहा जाता है।
उदाहरण –
अशुद्ध रूप – जाता वह बाज़ार है।
शुद्ध रूप – वह बाज़ार जाता है।
यद्यपि दोनों वाक्यों में सभी शब्द समान हैं किंतु पहले वाक्य में सही पदक्रम की कमी है, जबकि दूसरा वाक्य उचित पदक्रम के अनुसार है।
उदाहरण –
अशुद्ध रूप – शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा।
शुद्ध रूप – देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा।
अशुद्ध रूप – गाय का ताकतवर दूध होता है।
शुद्ध रूप – गाय का दूध ताकतवर होता है।
अशुद्ध रूप – अपनी बात आपको मैं बताता हूँ।
शुद्ध रूप – मैं आपको अपनी बात बताता हूँ।
अशुद्ध रूप – ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए।
शुद्ध रूप – विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए।
6. पुनरावृत्ति की अशुद्धियाँ/पुनरुक्ति दोष
एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ/भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है।
उदाहरण –
अशुद्ध रूप – वह बहुत जल्दी वापस लौट आया।
शुद्ध रूप – वह बहुत जल्दी लौट आया।
अशुद्ध रूप – जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं।
शुद्ध रूप – जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं।
अशुद्ध रूप – कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें।
शुद्ध रूप – आप मेरे घर आने की कृपा करें।
अशुद्ध रूप – प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।
शुद्ध रूप – प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।
7. विरामचिह्न संबंधी अशुद्धियाँ
कभी-कभी वाक्य में विराम चिह्न संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। जिसके कारण वाक्य को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। ये वाक्य की विरामचिह्न संबंधी अशुद्धियाँ कही जाती है।
उदारहण –
अशुद्ध रूप – गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है।
शुद्ध रूप – गुरुदेव! यह तो सरासर अन्याय है।
अशुद्ध रूप – धीरे धीरे ध्यान से चलो।
शुद्ध रूप – धीरे-धीरे ध्यान से चलो।
अशुद्ध रूप – वह काव्यसंग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है।
शुद्ध रूप – वह काव्यसंग्रह, जिसे मैंने लिखा है; वह छप रहा है।
अशुद्ध रूप – यह पुस्तक आपको कहाँ मिली।
शुद्ध रूप – यह पुस्तक आपको कहाँ मिली?
8. संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ
संज्ञा पद के प्रयोग में प्राय: दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं –
i) अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग
ii) अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग
i) अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग –
ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता न हो पर उनका प्रयोग किया जाए तो वहाँ अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियाँ हो जाती हैं।
उदाहरण –
अशुद्ध वाक्य – मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ।
शुद्ध वाक्य – मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ।
अशुद्ध वाक्य – अब विंध्याचल पर्वत हरा-भरा हो गया।
शुद्ध वाक्य – अब विंध्याचल हरा-भरा हो गया।
अशुद्ध वाक्य – ‘उत्साह’नामक शीर्षक निबंध अच्छा है।
शुद्ध वाक्य – ‘उत्साह’शीर्षक निबंध अच्छा है।
अशुद्ध वाक्य – राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया।
शुद्ध वाक्य – राजा अपने बल पर जीत गया।
अशुद्ध वाक्य – प्रात:काल के समय घूमना चाहिए।
शुद्ध वाक्य – प्रात:काल घूमना चाहिए।
अशुद्ध वाक्य – समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है।
शुद्ध वाक्य – समाज में अराजकता बढ़ रही है।
ii) अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग
ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग जो उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त अर्थात गलत हों उनके प्रयोग के कारण वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पदों की अशुद्धियाँ हो जाती हैं।
उदाहरण –
अशुद्ध वाक्य – गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही।
शुद्ध वाक्य – पैरो में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही।
अशुद्ध वाक्य – दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई।
शुद्ध वाक्य – दंगे में गोलियों की बौछार आ गई।
अशुद्ध वाक्य – रेडियो की उत्पत्ति किसने की।
शुद्ध वाक्य – रेडियो का आविष्कार किसने किया।
अशुद्ध वाक्य – आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है।
शुद्ध वाक्य – आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है।
अशुद्ध वाक्य – हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं।
शुद्ध वाक्य – हमारे देश के लोग मेहनती हैं।
9. सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ
हिंदी में कभी-कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं।
उदाहरण –
अशुद्ध वाक्य – मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं।
शुद्ध वाक्य – मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं।
अशुद्ध वाक्य – मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा।
शुद्ध वाक्य – मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
अशुद्ध वाक्य – मेरे को बाज़ार जाना है।
शुद्ध वाक्य – मुझे बाज़ार जाना है।
अशुद्ध वाक्य – तेरे को क्या चाहिए?
शुद्ध वाक्य – तुझे क्या चाहिए?
अशुद्ध वाक्य – दूध में कौन गिर गया?
शुद्ध वाक्य – दूध में क्या गिर गया?
अशुद्ध वाक्य – तुम तो तुम्हारा काम करो।
शुद्ध वाक्य – तुम तो अपना काम करो।
10. विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ
विशेषण का प्रयोग विशेष्य (संज्ञा व सर्वनाम) के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है। जो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं।
उदाहरण –
अशुद्ध वाक्य – घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि।
शुद्ध वाक्य – विष, शोभा, कुवृष्टि।
अशुद्ध वाक्य – धोबिन ने अच्छी चादरें धोईं।
शुद्ध वाक्य – धोबिन ने चादरें अच्छी धोईं।
अशुद्ध वाक्य – यह सबसे सुन्दरतम साड़ी है।
शुद्ध वाक्य – यह सुन्दरतम साड़ी है।
अशुद्ध वाक्य – आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला।
शुद्ध वाक्य – आज उसके रहस्य का राज खुला।
अशुद्ध वाक्य – उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है।
शुद्ध वाक्य – उनकी आजकल दयनीय हालत है।
अशुद्ध वाक्य – वह डाल महीन है।
शुद्ध वाक्य – वह डाल पतली है।
11. क्रिया संबंधी अशुद्धि
वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है।
उदाहरण –
अशुद्ध रूप – राम और सीता वन को गई।
शुद्ध रूप – राम और सीता वन को गए।
अशुद्ध रूप – उनकी बातें सुनते-सुनते कान पक गया।
शुद्ध रूप – उनकी बातें सुनते-सुनते कान पक गए।
अशुद्ध रूप – मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है।
शुद्ध रूप – मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है।
i) अनावश्यक क्रिया पद का प्रयोग –
जैसे –
अशुद्ध रूप – यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है।
शुद्ध रूप – यहाँ अशोभनीय वातावरण है।
अशुद्ध रूप – अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
शुद्ध रूप – अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
ii) आवश्यक क्रिया पद का प्रयोग न होना –
जैसे –
अशुद्ध रूप – वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है।
शुद्ध रूप – वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है।
अशुद्ध रूप – वह तो खाना और चाय पीकर सो गया।
शुद्ध रूप – वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया।
iii) अनुपयुक्त क्रिया पद –
जैसे –
अशुद्ध रूप – खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया।
शुद्ध रूप – खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया।
अशुद्ध रूप – मैं माताजी को खाना डालकर/देकर आई।
शुद्ध रूप – मैं माताजी को खाना परोसकर आई।
iv) हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है –
जैसे –
अशुद्ध रूप – दान दिया।
शुद्ध रूप – दान किया।
अशुद्ध रूप – प्रतीक्षा देखना।
शुद्ध रूप – प्रतीक्षा करना।
अशुद्ध रूप – प्रयोग होना।
शुद्ध रूप – प्रयोग करना।
अशुद्ध रूप – प्रश्न पूछना।
शुद्ध रूप – प्रश्न करना।
v) स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है –
जैसे –
अशुद्ध रूप – वह खाना खावेगा।
शुद्ध रूप – खाना खायेगा।
अशुद्ध रूप – उसने जैसी करी है, मैं नहीं कर सकता।
शुद्ध रूप – उसने जैसा किया है, मैं नहीं कर सकता।
12. क्रियाविशेषण संबंधी अशुद्धियाँ
अशुद्ध वाक्य – विद्यालय के दाएँ बड़ा-सा मैदान है।
शुद्ध वाक्य – विद्यालय की दाईं ओर बड़ा-सा मैदान है।
अशुद्ध वाक्य – भिखारी को थोड़ा चावल दे दो।
शुद्ध वाक्य – भिखारी को थोड़े चावल दे दो।
अशुद्ध वाक्य – राम दिनों-दिन मेहनत करता है।
शुद्ध वाक्य – राम दिनों-रात मेहनत करता है।
अशुद्ध वाक्य – जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे।
शुद्ध वाक्य – जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
अशुद्ध वाक्य – पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है।
शुद्ध वाक्य – पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है।
13. कारक संबंधी अशुद्धियाँ –
वाक्यों में कारक संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं, जिस कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इन अशुद्धियों को कारक संबंधी अशुद्धियाँ कहा जाता है।
i) कर्ताकारक संबंधी अशुद्धि –
भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ‘ने’चिह्न का प्रयोग किया जाता है।
जैसे –
अशुद्ध रूप – मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली।
शुद्ध रूप – मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली।
ii) कर्मकारक संबंधी अशुद्धि –
किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्त्व दिया जाता है, तो वहाँ कर्मकारक के चिह्न ‘को’ का प्रयोग किया जाता है; अन्यथा उसका प्रयोग नहीं किया जाता।
जैसे –
अशुद्ध रूप – वह लड़का पीटता है।
शुद्ध रूप – वह लड़के को पीटता है।
अशुद्ध रूप – मैं शीतल जल को पी रहा हूँ।
शुद्ध रूप – मैं शीतल जल पी रहा हूँ।
iii) करणकारक संबंधी अशुद्धि –
जैसे –
अशुद्ध रूप – वह बस पर यात्रा कर रहा है।
शुद्ध रूप – वह बस से यात्रा कर रहा है।
iv) सम्प्रदानकारक संबंधी अशुद्धि –
सम्प्रदान कारक के दो चिह्न हैं ‘के लिए’और ‘को’, यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है।
जैसे –
अशुद्ध रूप – पंडितजी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई।
शुद्ध रूप – पंडितजी ने भक्तों को कथा सुनाई।
अशुद्ध रूप – शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया।
शुद्ध रूप – शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया।
v) अपादानकारक संबंधी अशुद्धि
अशुद्ध रूप – वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है।
शुद्ध रूप – वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है।
अशुद्ध रूप – लड़की झूले पर से गिर गई।
शुद्ध रूप – लड़की झूले से गिर गई।
vi) संबंधकारक संबंधी अशुद्धि –
अशुद्ध रूप – बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता।
शुद्ध रूप – बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता।
अशुद्ध रूप – राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है।
शुद्ध रूप – राधाकृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है।
नोट – ‘राधाकृष्ण’ सामासिक पद है अतः इसके चिह्न लुप्त हो गए हैं।
vi) अधिकरणकारक संबंधी अशुद्धि –
अशुद्ध रूप – आज बजट के ऊपर बहस होगी।
शुद्ध रूप – आज बजट पर बहस होगी।
अशुद्ध रूप – किसान ने खेत पर बीज बोया है।
शुद्ध रूप – किसान ने खेत में बीज बोया है।
अशुद्ध रूप – घर पर सब कुशल हैं।
शुद्ध रूप – घर में सब कुशल हैं।